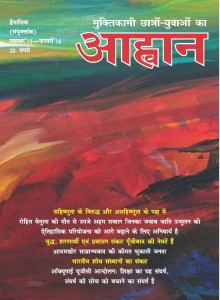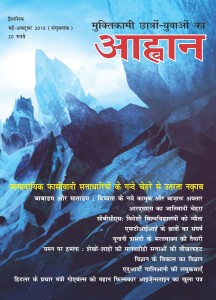12 जून 2015 को शुरू हुआ पुणे के फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डिया (भारत फिल्म और टेलीविजन संस्थान) के छात्रों का संघर्ष 139 दिन लम्बी चली हड़ताल के ख़त्म होने के बावजूद आज भी जारी है। 139 दिनों तक चली इस हड़ताल के दौरान देश भर के छात्रों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, फिल्मकारों, मज़दूर कार्यकर्ताओं और आम जनता ने खुलकर एफ.टी.आई.आई. के छात्रों की हड़ताल का समर्थन किया। 24 फिल्मकारों ने अपने राष्ट्रीय पुरस्कार वापिस किये जिनमें एफ.टी.आई.आई. के पूर्व अध्यक्ष सईद अख़्तर मिर्ज़ा, ‘जाने भी दो यारो’ फिल्म बनाने वाले कुंदन शाह, संजय काक आदि जैसे फिल्मकार शामिल थे। बार-बार सरकार के सामने अपनी माँगों को रखने और उनसे उन्हें संज्ञान में लेते हुए उनकी सुनवाई करने की अपीलों के बावजूद भी मोदी की फ़ासीवादी सरकार ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलते हुए इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखी। नरेन्द्र दाभोलकर, गोविन्द पानसरे और कलबुर्गी जैसे बुद्धिजीवियों की हत्या, दादरी में अख़लाक की हत्या, देश में बढ़ रहे फासीवादी आक्रमण और संघी गुण्डों की मनमर्ज़ी की पृष्ठभूमि में एफ.टी.आई.आई.के छात्रों के संघर्ष को संघ के भगवाकरण और हिन्दुत्व के मुद्दे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। एफ.टी.आई.आई. की स्वायत्तता पर हमला देश के शिक्षण संस्थानों और कला के केन्द्रों के भगवाकरण के फ़ासीवादी एजेण्डे का ही हिस्सा है। गजेन्द्र चौहान, अनघा घैसास, राहुल सोलपुरकर, नरेन्द्र पाठक, शैलेश गुप्ता जैसे लोगों की एफ.टी.आई.आई. सोसाइटी में नियुक्ति की खबर के बाद 12 जून को शुरू हुई हड़ताल ने देश के सभी छात्रों को भगवाकरण की इस मुहिम के ख़िलाफ़ एकजुट कर दिया।