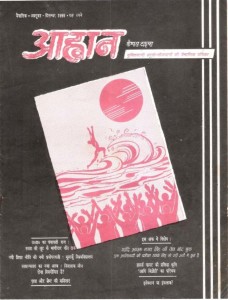रिचर्ड लेविंस – विज्ञान और समाज को समर्पित द्वन्द्वात्मक जीववैज्ञानिक
एक मार्क्सवादी होने के नाते लेविंस केवल एक क्लर्क वैज्ञानिक बनने में यकीन नहीं रखते थे, उनका मानना था कि विज्ञान एक सामाजिक सम्पत्ति है और इसका अध्ययन बिना उस समाज को बनाने वाली बहुसंख्यक जनता के जीवन को शोषण से मुक्त किये और बिना समृद्ध बनाने के लिए समर्पित किये व्यर्थ है। उनका कहना था कि विज्ञान को समझना समाज और दुनिया को बदलने के लिए ज़रूरी है क्योंकि बिना बदलाव के विज्ञान को समझे बदलाव ला पाना सम्भव नहीं है ।