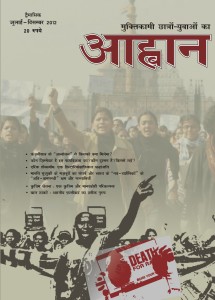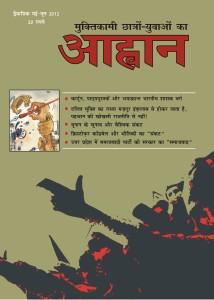सोशल मीडिया के बहाने जनता, विचारधारा और तकनोलॉजी के बारे में कुछ बातें
समाज की एक भारी मध्यवर्गीय आबादी इण्टरनेट-फेसबुक पर बैठी हुई सामाजिक जीवन के यथार्थ से बाहर एक आभासी यथार्थ में जीने का आदी हो जाती है। वह वस्तुत: भीषण सामाजिक अलगाव में जीती है, पर फेसबुक मित्रों का आभासी साहचर्य उसे इस अलगाव के पीड़ादायी अहसास से काफी हद तक निजात दिलाता है। बुर्ज़ुआ समाज की भेड़चाल में वैयक्तिक विशिष्टता की मान्यता का जो संकट होता है, पहचान-विहीनता या अजनबीपन की जो पीड़ा होती है, उससे फेसबुक-साहचर्य, एक दूसरे को या उनके कृतित्व को सराहना, एक दूसरे के प्रति सरोकार दिखाना काफी हद तक राहत दिलाता है। यानी यह भी एक तरह के अफीम की भूमिका ही निभाता है। यह दर्द निवारक का काम करता है और एक नशे का काम करता है, पर दर्द की वास्तविक जड़ तक नहीं पहुँचाता। इस तरह अलगाव के विरुद्ध संघर्ष की हमारी सहज सामाजिक चेतना को यह माध्यम पूँजीवादी व्यवस्था-विरोधी सजग चेतना में रूपांतरित हो जाने से रोकता है। साथ ही, फेसबुक, टि्वटर और सोशल मीडिया के ऐसे तमाम अंग-उपांग हमें आदतन अगम्भीर और काहिल और ठिठोलीबाज भी बनाते हैं। खुशमिजाजी अच्छी चीज है, पर बेहद अंधकारमय और चुनौतीपूर्ण समय में भी अक्सर चुहलबाजी के मूड में रहने वाले अगम्भीर लोग न केवल अपनी वैचारिक क्षमता, बल्कि अपनी संवेदनशीलता भी खोते चले जाते हैं।