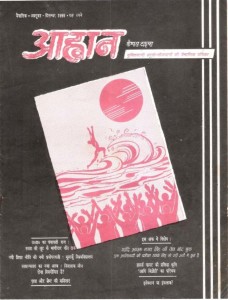तेलतुम्बडे यहाँ असत्य वचन का सहारा ले रहे हैं कि उन्होंने मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद के मिश्रण या समन्वय की कभी बात नहीं की या उसे अवांछित माना है। 1997 में उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में एक पेपर प्रस्तुत किया, ‘अम्बेडकर इन एण्ड फॉर दि पोस्ट-अम्बेडकर दलित मूवमेण्ट’। इसमें दलित पैंथर्स की चर्चा करते हुए वह लिखते हैं, “जातिवाद का असर जो कि दलित अनुभव के साथ समेकित है वह अनिवार्य रूप से अम्बेडकर को लाता है, क्योंकि उनका फ्रेमवर्क एकमात्र फ्रेमवर्क था जो कि इसका संज्ञान लेता था। लेकिन, वंचना की अन्य समकालीन समस्याओं के लिए मार्क्सवाद क्रान्तिकारी परिवर्तन का एक वैज्ञानिक फ्रेमवर्क देता था। हालाँकि, दलितों और ग़ैर-दलितों के बीच के वंचित लोग एक बुनियादी बदलाव की आकांक्षा रखते थे, लेकिन इनमें से पहले वालों ने सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन के उस पद्धति को अपनाया जो उन्हें अम्बेडकरीय दिखती थी, जबकि बाद वालों ने मार्क्सीय कहलाने वाली पद्धति को अपनाया जो कि हर सामाजिक प्रक्रिया को महज़ भौतिक यथार्थ का प्रतिबिम्बन मानती थी।………… अब पाठक ही बतायें कि तेलतुम्बडे जो दावा कर रहे हैं, क्या उसे झूठ की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? क्या यहाँ पर ‘अम्बेडकरीय’ और ‘मार्क्सीय’ दोनों को ‘अम्बेडकरवाद’ और ‘मार्क्सवाद’ के अर्थों में यानी ‘दो विचारधाराओं’ के अर्थों में प्रयोग नहीं किया गया है? फिर तेलतुम्बडे यह आधारहीन और झूठा दावा क्यों करते हैं कि उन्होंने कभी ‘अम्बेडकरवाद’ शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वह नहीं मानते कि ऐसी कोई अलग विचारधारा है? क्या यहाँ पर उन्होंने अम्बेडकर की विचारधारा और मार्क्स की विचारधारा और उनके मिश्रण की वांछितता की बात नहीं की? हम सलाह देना चाहेंगे कि तेलतुम्बडे के कद के एक जनपक्षधर बुद्धिजीवी को बौद्धिक नैतिकता का पालन करना चाहिए और इस प्रकार सफ़ेद झूठ नहीं बोलना चाहिए।