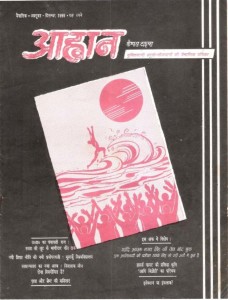यह योजना महज चुनावी कार्यक्रम नहीं बल्कि व्यापारियों का मुनाफा और बढ़ाने की योजना है
यह बात सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) में कई कमियाँ हैं। सबसे बड़ी कमी है ग़रीबी रेखा का निर्धारण ही सही तरीके से नहीं किया गया है। मौजूदा ग़रीबी रेखा हास्यास्पद है। उसे भुखमरी रेखा कहना अधिक उचित होगा। पौष्टिक भोजन के अधिकार को जीने के मूलभूत संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया जाना चाहिए तथा इसके लिए प्रभावी क़ानून बनाये जाने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ही पुनर्गठन किया जाए और अमल की निगरानी के लिए जिला स्तर तक प्रशासनिक अधिकारी के साथ-साथ लोकतान्त्रिक ढंग से चुनी गयी नागरिक समितियाँ हों। पर किसी पूँजीवादी व्यवस्था से ऐसी उम्मीद कम ही है; भारत समेत पूरी दुनिया जिस आर्थिक मंदी से गुज़र रही है ऐसे समय में ऐसी नीतियों का बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस देश के आम लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सही मायने में लागू करवाने के लिए छात्र-नौजवानों और नागरिकों का दायित्व है कि ऐसी योजनाओं की असलियत को उजागर करते हुए देश की जनता को शासक वर्ग की इस धूर्ततापूर्ण चाल के बारे में आगाह करें जिससे कि एक कारगर प्रतिरोध खड़ा किया जा सके।