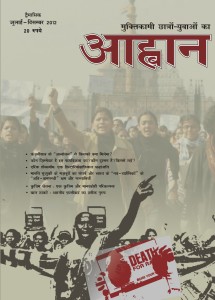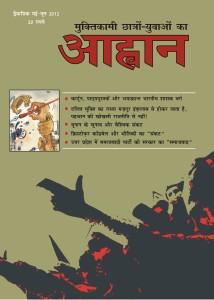असम में एनआरसी पर ‘ललकार’ के भाषाई व राष्ट्रीय अस्मितावाद के शिकार साथियों की ग़लत अवस्थिति पर ‘आह्वान’ की ओर से 14 दिसम्बर 2019 को डाली गयी टिप्पणी
इस फ़र्क़ को समझने में कई प्रबुद्ध और प्रगतिशील लोगों से भी ग़लती हो रही है। मगर हैरत की बात तो यह है कि अपने को वाम क्रान्तिकारी कहने वाले कुछ लोग भी न सिर्फ़ असम में हो रहे कैब के विरोध के पीछे की राजनीति को समझ नहीं रहे बल्कि भाषाई अस्मितावाद और अन्धराष्ट्रवाद के अपने चश्मे से देखकर उसकी भी घोर अनर्थकारी व्याख्या पेश कर रहे हैं। वैसे, इसमें ज़्यादा हैरत की बात भी नहीं है। पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान इनका भाषाई अस्मितावाद और राष्ट्रवादी भटकाव जिस दिशा में बढ़ता रहा है उसे यहीं तक जाना था। दूसरे, ये भी वाम आन्दोलन के अनेक हलक़ों में व्याप्त इस बीमारी से बुरी तरह ग्रस्त हैं जिसके चलते लोग इतिहास, राजनीति, भाषा, संस्कृति आदि की अधकचरी जानकारी लिये हुए हर बात पर ज्ञान बघारते रहते हैं, बिना यह समझे कि इसकी दूरगामी परिणतियाँ कितनी भयंकर होंगी।