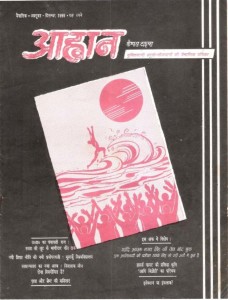सारदा चिटफण्ड घोटालाः सेंधमार, लुटेरे पूँजीवाद का प्रातिनिधिक उदाहरण
निम्न पूँजीपति वर्ग के लोगों ने लाखों की तादाद में इन मज़ाकिया स्कीमों पर भरोसा क्यों किया इसे समझने के लिए इस वर्ग के चरित्र को समझने की भी ज़रूरत है। यह वर्ग न पूरी तरह आबाद होता है और न ही पूरी तरह बरबाद होता है। नतीजतन, इसकी राजनीतिक वर्ग चेतना भी अधर में लटकी होती है। अपनी राजनीतिक माँगों के लिए संगठित होने और सरकार की नीतियों के ख़िलाफ जनता के अन्य मेहनतकश हिस्सों के साथ संगठित होकर आवाज़ उठाने की बजाय अधिकांश मामलों में वह पूँजीवादी व्यवस्था के पैरोकारों द्वारा पेश किये जा रहे दावों और वायदों पर भरोसा कर बैठता है। और जब उसे इसका ख़ामियाज़ा भुगताना पड़ता है तो वह काफ़ी छाती पीटता है और शोर मचाता है। सारदा ग्रुप जैसी फ्रॉड कम्पनियों की स्कीमों के निशाने पर ये ही वर्ग होते हैं, जो परिवर्तन और बदलाव की मुहिम के ढुलमुलयकीन मित्र होते हैं। जब परिवर्तन की ताक़तें उफान पर होती हैं, तो ये उनके पीछे चलते हैं और जब माहौल यथास्थितिवादी ताक़तों के पक्ष में होता है, तो ये अपने निजी, व्यक्तिगत हित साधने में व्यस्त रहते हैं और व्यवस्था को एक प्रकार से मौन समर्थन देते हैं।