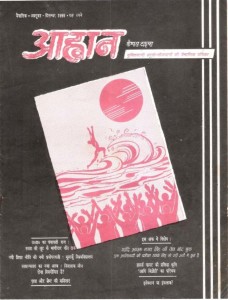राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की असली जन्मकुण्डली
संघ का सांगठनिक ढांचा भी मुसोलिनी और हिटलर की पार्टी से हूबहू मेल खाता है। इटली का फ़ासीवादी नेता मुसोलिनी जनतंत्र का कट्टर विरोधी था और तानाशाही में आस्था रखता था। मुसोलिनी के मुताबिक “एक व्यक्ति की सरकार एक राष्ट्र के लिए किसी जनतंत्र के मुकाबले ज़्यादा असरदार होती है।” फ़ासीवादी पार्टी में ‘ड्यूस’ के नाम पर शपथ ली जाती थी, जबकि हिटलर की नात्सी पार्टी में ‘फ़्यूहरर’ के नाम पर। संघ का ‘एक चालक अनुवर्तित्व’ जिसके अन्तर्गत हर सदस्य सरसंघचालक के प्रति पूर्ण कर्मठता और आदरभाव से हर आज्ञा का पालन करने की शपथ लेता है, उसी तानाशाही का प्रतिबिम्बन है जो संघियों ने अपने जर्मन और इतावली पिताओं से सीखी है। संघ ‘कमाण्ड स्ट्रक्चर’ यानी कि एक केन्द्रीय कार्यकारी मण्डल, जिसे स्वयं सरसंघचालक चुनता है, के ज़रिये काम करता है, जिसमें जनवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। यही विचारधारा है जिसके अधीन गोलवलकर (जो संघ के सबसे पूजनीय सरसंघचालक थे) ने 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद् के प्रथम अधिवेशन को भेजे अपने सन्देश में भारत में संघीय ढाँचे (फेडरल स्ट्रक्चर) को समाप्त कर एकात्म शासन प्रणाली को लागू करने का आह्वान किया था। संघ मज़दूरों पर पूर्ण तानाशाही की विचारधारा में यक़ीन रखता है और हर प्रकार के मज़दूर असन्तोष के प्रति उसका नज़रिया दमन का होता है। यह अनायास नहीं है कि इटली और जर्मनी की ही तरह नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में मज़दूरों पर नंगे किस्म की तानाशाही लागू कर रखी है। अभी हड़ताल करने पर कानूनी प्रतिबन्ध तो नहीं है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर प्रतिबन्ध जैसी ही स्थिति है; श्रम विभाग को लगभग समाप्त कर दिया गया है, और मोदी खुद बोलता है कि गुजरात में उसे श्रम विभाग की आवश्यकता नहीं है! ज़ाहिर है-मज़दूरों के लिए लाठियों-बन्दूकों से लैस पुलिस और सशस्त्र बल तो हैं ही!